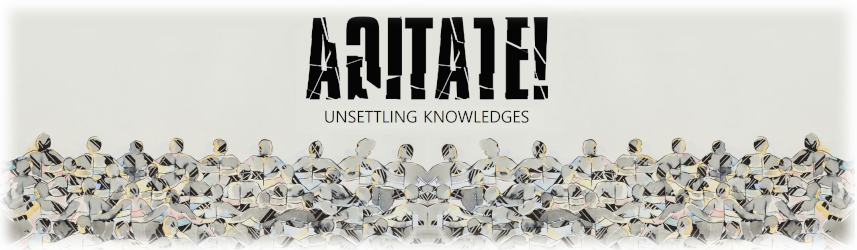जसिन्ता को पढ़ने पर …
After Reading Jacinta1
विशाल जामकर और ऋचा नागर
Vishal Jamkar and Richa Nagar
किसी ने नहीं देखा मुझे
जब आँगन की मिट्टी को
सीमेंट का कवच पहनाया गया
मैं मिट्टी को समझाता रहा
मज़बूत नींव के लिए
ज़रूरी है उसका मरना,
मगर मैंने देखा
एक-एक कर
फूलों को भी मरते हुए।
– जसिंता केरकेट्टा2
No one ever saw me
As the soil of the courtyard
Was draped in the armour of cement.
I kept telling the soil
it was necessary
for it to die, to make way for a strong foundation.
But then I witnessed
even the flowers
dying one by one.
– Jacinta Kerketta3
कैसा अजब है न यह मिट्टी, फूल, और सीमेंट का खेल भी? जहाँ एक तरफ़ सीमेंट मिट्टी के सोंधेपन को ख़त्म करके उसे एक श्वाँस-रहित शिला बना देता है, वहीं दूसरी तरफ़ मिट्टी का हरण करके उसे सीमेंट के रूप में पूजने वाला इंसान मरकर खुद माटी और फूल बन जाता है।
सच पूछिए तो सीमेंट और माटी का यह द्वन्द, जिसका बखान जसिन्ता अपनी कविता में करती हैं, अब द्वन्द भी कहाँ रहा; जगह-जगह सीमेंट ने मिट्टी का गला घोंटकर उसे भारी-भरकम मात दे दी है! जहाँ नज़र उठाकर देखो वहाँ पहाड़ और जंगल खुद-खुद कर चुक चुके हैं, और बड़ी-बड़ी इमारतें सीना ताने खड़ी हैं – मानो जँगलों, फूलों, और गाँवों को रौंदने का जश्न मना रही हों!
हो सकता आप कभी बस्तर न गए हों, लेकिन अगर आपका कभी उधर से गुज़रना हो तो देखिएगा कि जब बस्तर के डामरी रास्ते से होकर गाँव में अंदर की ओर मुड़ते हैं तो आज भी पुरानी संस्कृति के अवशेष हर तरफ़ बिखरे पड़े हैं – जैसे, पुराने मकानों में, पूजा-स्थलों में, बुज़ुर्गों के मुँह के निकलती कहानियों में।
हममें से एक (ऋचा) का तो कभी बस्तर जाना नहीं हुआ, लेकिन ख़ुशकिस्मती से विशाल को छत्तीसगढ़ के उत्तर बस्तर कांकेर ज़िले के भानुप्रतापपुर विकास खंड में छह साल जीने और सीखने को बहुत कुछ मिला। दरअसल, उस इलाक़े में नक्सली विद्रोह, बस्तरिया जीवन-संस्कृति, और आदिवासी बाहुल्य के होने के कारण विशाल को उस क्षेत्र में बेहद रूचि पैदा हो चुकी थी। इसलिए जिस स्वयंसेवी संस्था में विशाल कार्यरत था, वहाँ से जब उसे बस्तर में रहकर काम करने का मौक़ा दिया गया, तो वह उस अवसर पर ख़ुशी से झपट पड़ा। इस काम के तहत उसे भानुप्रतापपुर विकास खंड में अनेक साथियों के साथ मिलकर ११० गाँवों में महिला स्वयं-सहायता समूह बनाने का मौक़ा मिला और फिर यहीं की तक़रीबन १०,००० दलित एवं आदिवासी महिलाओं ने महिला शक्ति संगठन-भानुप्रतापपुर की नींव डाली। यह संगठन महिलाओं एवं उनके परिवारों के बीच आजीविका तथा लिंग भेद एवं अन्य पहलुओं से जुड़े अधिकारों को लेकर संघर्ष कर रहा है। इस काम में मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, कृषि, महिला एवं बाल विकास जैसी विविध सरकारी योजनाओं को योग्य व्यक्तियों तक पहुँचाना शामिल है। जिन लोगों तक यह विकास योजनाएं पहुँचनी चाहिए या जहाँ-जहाँ लोगों को इनका फ़ायदा उठाने में दिक़्क़त पेश आई, वहाँ-वहाँ संगठन ने उन योजनाओं को ज़रूरतमंदों तक पहुँचाने के लिए दम लगाकर मेहनत की है। ग़ौरतलब है कि यह सारा काम काफ़ी हद तक तथाकथित “अशिक्षित” आदिवासी और दलित महिलाओं की बदौलत हुआ है। इन्हीं औरतों ने तमाम गाँवों में मनरेगा से सम्बद्ध जागरूकता प्रदान करने के साथ-साथ तकनीकी योजनाएँ बनाने में विकास खंड के अभियंता एवं ग्राम पंचायतों की भी भरपूर मदद की।
इस पूरे काम का बखान करते हुए हमारे भीतर सिहरन-सी दौड़ जाती है। बार-बार यही याद आता है कि किस तरह हमारे जैसे “पढ़े-लिखे” लोगों की तथाकथित उच्च शिक्षा हमें अक्सर यही सिखलाती है कि गाँव-देहात के “अनपढ़” लोग खुद कुछ करने में सक्षम हैं ही नहीं। कि जब-तक किसी संस्था के ज़रिये कुछ डिग्री-पास रहनुमा इनको रास्ता दिखने के लिए प्रकट नहीं होंगे, तब तक “ये बेचारे” अँधेरे में बैठे रहेंगे! कितने ही तथाकथित उच्च-शिक्षा प्राप्त लोग इस मुग़ालते में रहते हैं कि उनके जैसे मसीहे ही अनपढ़ों को उनके ही समाज की बुरी आदतों से छुटकारा दिला सकते हैं, कि वे ही इन्हें इनके अपने संसाधनों का उचित उपयोग करना सिखा सकते हैं, वग़ैरह, वग़ैरह!
विशाल को जल्द ही समझ में आ गया कि ऐसी न जाने कितनी ही धारणाओं और अवधारणाओं को—जो हमारे जातिवादी, वर्गवादी, सम्प्रदायवादी समाज में कूट-कूटकर भरी हैं—उसे तिलांजलि देनी होगी। काश, औपचारिक शिक्षा देने वाले हमारे बड़े-बड़े स्कूल और कॉलेज हमें यह सिखा पाते कि नैसर्गिक और मानवीय लेन-देन के अंतर्गत ऐसा बहुत कुछ सीखा जाता है जो उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रचलित अकादमिक पद्धतियों के ज़रिये सीखना या सोखना असंभव है। लेकिन हमारी दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी शायद यही है कि ऐसी शिक्षा को ग्रहण करने के लिए हमें जो आँखें, जो कान, जो मन चाहिए वही हमारे स्कूल और कॉलेज हमसे सबसे पहले छीन लेते हैं। विशेषग्यताओं के नाम पर हम “उच्च-शिक्षित” अपनी ही कल्पनाओं और ज़ुबानों को बेहद सीमित दायरों में क़ैद करके अक्सर अपनी पूरी-पूरी ज़िन्दगियाँ बिता देते हैं।
विकास और शिक्षा की इस गहरी और ज़हरीली घुसपैठ को दुनिया के हर हिस्से में देखा जा सकता है। हम दोनों ने अपने लम्बे काम और सम्बन्धों के सन्दर्भ में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ग्रामीण जीवन पर इस घुसपैठ के असर खूब देखे हैं। कदाचित सबसे बड़ा असर तो यही है कि हमारी अपनी औपचारिक और स्कूली कुशिक्षा का मोटा-सा जामा आज पूरी-की-पूरी सामाजिक और राजनैतिक व्यवस्था पर चढ़ चुका है। यह भारी-भरकम जामा सीमेंट के उसी कवच की तरह है जो मिट्टी का दम घोंट देता है – इस कवच के ख़िलाफ़ अपने अंतर-मन में विद्रोह किये बिना हमारे गाँवों की बेतरह उजाड़ी जा रही संस्कृतियों के बारे में ईमानदारी और गहराई से जानना मुमकिन है ही नहीं। देहात के त्योहारों में, बाज़ारों में, फसल-चक्रों में, रिश्तों में महज़ वहाँ की अपनी संस्कृति ही नहीं झलकती, बल्कि इन सबमें वहाँ की अपनी धरती-पानी-हवा से उपजा और पला गहरा ज्ञान भी समाहित रहता है। यहाँ हमारा यह आशय क़तई नहीं है कि इन जगहों में होने वाले मेले-हाट-बाज़ारों के मायने और तरीक़े दशकों से जस-के-तस हैं, या फिर ग्रामीणों और आदिवासियों की संस्कृति ही आदर्श संस्कृति है, जिसमें सब कुछ हमेशा सही और न्यायपूर्ण है।
जब ऋचा ने विशाल के साथ जसिन्ता केरकेट्टा का AGITATE! के लिए भेजा लेख साझा किया तो उस लेख को पढ़ने के बाद विशाल के मन में छत्तीसगढ़ की तमाम यादों के तार झनझना उठे – ऐसी यादें जो शहरी और ग्रामीण संस्कृतियों के ज्ञान के टकराव से ही नहीं जुड़ीं हैं, बल्कि इंसानी रिश्तों को लेकर रोज़ की बस्तरिया रीतियों से भी गुँथी हुई हैं। ये रीतियाँ पूरा जीवन जीने का ऐसा सामान हैं जिनके बारे में अगर हम खुले दिलो-दिमाग़ से जानने की कोशिश करें तो निश्चित ही शहरी समाज की मानसिकताओं और अवधारणाओं पर गम्भीरता के विचार करने को मजबूर होंगे।
घोटुल तक पहुँचना
गाँवों में वक़्त बिताने के साथ-साथ विशाल ने गोंड समाज के बारे में पढ़ना भी शुरू किया। अक्सर, दूसरे कामों से फ़ुरसत निकालकर बुज़ुर्ग महिलाओं और पुरुषों से बात करने में उसे सुकून मिलने लगा। तमाम बातें होती थीं – गोंड समाज के बारे में, संस्कृति के बारे में, फसल के बारे में… इन सब चर्चा में एक विषय था जिसका ज़िक्र तो अक्सर होता था लेकिन जिसपर खुलकर बात नहीं होती थी – घोटुल! जैसे-जैसे विशाल की उत्सुकता बढ़ी, वैसे-वैसे उसने घोटुल पर भी अध्ययन करना शुरू किया, लेकिन ऐसे कितने ही सवाल मन में आते थे जिनके जवाब किताबों में नहीं मिलते थे।
क्षेत्र में कुछ महीने काम करने के बाद विशाल का कई लोगों से क़रीबी रिश्ता बनने लगा। वैसे भी, गोंड समाज में शादी-त्योहारों में जाकर सूअर का माँस और छिंदरस पी लो तो रिश्ता गहरा हो ही जाता है! ऐसे ही रोज़ाना के साथ-साथ उठने-बैठने-बतियाने के बाद विशाल ने परवी गाँव की कौसल्या से थोड़ा झिझकते हुए सवाल किया, “दीदी, आपसे एक बात पूछूँ, ये घोटुल क्या होता है? जबसे यहाँ आया हूँ, काफ़ी लोगों से इसके बारे में सुना है, लेकिन किसी से इसके बारे में ठीक से बात नहीं हुई है। क्या मुझे आप घोटुल के बारे में कुछ बतायेंगी?”
विशाल की आवाज़ में शायद कौतूहल और सम्मान था, वर्ना अक्सर शहरियों के मुख से ऐसे सवाल इस तरह उठते हैं कि गोंडी लोग या तो इस विषय में कुछ भी साझा करने से कतराते हैं, या फिर ख़ुद को अपमानित महसूस करते हैं। इस बैठक के बाद भी विशाल का यह सवाल सुनकर पहले-पहल तो कमरे में मौजूद सभी औरतों ने लाज से मुँह मोड़कर हँसते हुए अपने पल्लुओं में चेहरे छिपा लिये। बाद में जब विशाल ने यही चर्चा मर्दों के बीच उठानी चाही तो उन्होंने भी हँसकर बात टाल दी।
जितना ही लोग उसके सवालों को टालते थे, घोटुल को समझने की विशाल की छटपटाहट उतनी ही बढ़ती जाती थी। इसलिए विशाल और भी शिद्दत से कोशिश करने लगा – अकेले में बात करके दीदियों और भैय्यायों को बार-बार यह विश्वास दिलाने की कोशिश करता कि वह घोटुल को केवल युवाओं के लैंगिक मिलन के तरीक़े के रूप में छोटा करके नहीं देखता। और यह भी, कि यदि घोटुल इस मिलन का मात्र एक साधन-भर है तो भी विशाल को उसमें कुछ अनुचित नहीं लगता।
विकास की राजनीति ने औपचारिक शिक्षा के ज़रिये शहर और गाँव, तथा शहरी और आदिवासी लोगों के रिश्तों को कुछ इस तरह से तोड़ा-मरोड़ा है कि गाँव के लोग अक्सर नगर-वासियों के मुँह से निकलने वाले लफ़्ज़ों के आधार पर उनकी बात पर भरोसा नहीं कर पाते! जब बाक़ी शरीर की ज़बान और हाव-भावों से उन्हें सहजता और ईमानदारी दिखती है तभी खुलते हैं।
यह भी ग़ौरतलब है कि विशाल को इस विषय में अपने इर्द-गिर्द मौजूद लोगों से गहराई से जान पाने में इतना समय क्यों लगा? क्या मूलतः शहर का होने के कारण वह उनसे घोटुल के बारे में खुलकर बात करने का हक़ गवाँ चुका था? क्या इस विषय में की गई हर पूछताछ उनको यही याद दिलाती थी कि कैसे घोटुल जैसी महत्त्वपूर्ण और तमाम मायनों से परिपूर्ण संस्था को तथाकथित शिक्षित वर्ग ने अपनी बातों में इतना छोटा कर दिया है कि वह महज़ एक पुरातन रीति या बीती बात बन गयी है जिसका ज़िक्र केवल मज़ाक़ में तब्दील होकर रह जाता है?
ख़ैर, जब विशाल ने अपनी दीदियों और भैय्यायों का विश्वास जीत लिया तो घोटुल पर सहजता से चर्चाएँ होने लगीं। जिन आदिवासी महिलाओं को अक्सर अशिक्षित घोषित कर दिया जाता है, उन्हीं महिलाओं को खुलकर घोटुल जैसे विषय पर बात करता देखकर किसी शहरी डिग्री-धारी को भ्रम हो सकता है कि वह जे.एन. यू. अथवा हार्वर्ड की किसी इंटेलेक्चुअल सेमिनार में बैठा हुआ है। विशाल को गहराई से समझ में आने लगा कि नैसर्गिक अनुभूति से निकला हुआ चिंतन और ईमानदारी से व्यक्त विचार कितने अद्भुत होते है, और यही विचार हमारी दुनिया में व्याप्त ग़ैरबराबरियों और हिंसा से टक्कर लेने की किस क़दर ताक़त रखते हैं। यही नहीं, वह यह भी समझ पाया कि हमारी अनेक दुनियाओं में ज्ञान का न जाने कितना ऐसा भंडार है जहाँ तक हम अगर कभी पहुँच सकते हैं तो सिर्फ़ एक दोस्त बनकर घने रिश्तों के दम पर, न कि विशेषज्ञ बनकर अपनी ऊंची शिक्षा या डिग्री के दम्भ पर। 
विशाल की घोटुल डायरी
अगर आपको संक्षेप में घोटुल के बारे में बताऊँ तो गोंड जनजाति, भारत की एक प्रमुख जनजाति हैं। गोंड भारत के कटि प्रदेश— विंध्यपर्वत, सतपुड़ा पठार, छत्तीसगढ़ मैदान में दक्षिण तथा दक्षिण-पश्चिम में गोदावरी नदी तक फैले हुए पहाड़ों और जंगलों— में रहनेवाली द्रविड़ मूल की एक जनजाति है, जो संभवत: पाँचवीं-छठी शताब्दी में दक्षिण से गोदावरी के तट को पकड़कर मध्य भारत के पहाड़ों और जंगलों में फैल गई। कहा जाता है कि गोंड समाज के आयोजक लिंगो पेन ने गोंड समाज के ७५० कुलों को गोत्र में आयोजित किया एवं सामाजिक शिक्षा प्रदान करने के लिए घोटुल की स्थापना की।
साधारणतः घोटुल गाँव के किनारे बनी एक मिट्टी की झोपड़ी होती है। यह छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों और भारत में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के पड़ोसी क्षेत्रों में गोंड और मुरिया जनजातीय जीवन का एक अभिन्न अंग है। घोटुल गोंड समाज के सामाजिक और धार्मिक जीवन का केंद्र है। गोंड किंवदंती के अनुसार, सर्वोच्च देवता लिंगो ने पहला घोटुल बनाया। इसके सदस्यों के रूप में अविवाहित युवा लड़कों और लड़कियों के साथ एक बड़ा सूत्रधार होता है। घोटुल की महिला सदस्यों को मोटियारिन कहा जाता है, जबकि पुरुष सदस्यों को चेलिक कहा जाता है। उनके नेताओं को क्रमशः बेलोसा और सरदार कहा जाता है। सदस्यों को स्वच्छता, अनुशासन और कड़ी मेहनत का पाठ पढ़ाया जाता है। उन्हें अपनी उपस्थिति पर गर्व करना और स्वयं का, अपना तथा अपने बड़ों का, सम्मान करना सिखलाया जाता है। इसी तरह उन्हें सार्वजनिक सेवा का मंत्र भी दिया जाता है।
हर शाम को जवान लड़के-लड़कियाँ धीरे-धीरे घोटुल के नज़दीक इकट्ठा होने लगते हैं और सब के सब समूह में गाते हुए घोटुल तक पहुँचते हैं। घोटुल में कुछ अधेड़ लोग भी आते हैं, लेकिन वे दूर बैठकर ही नाच-गाना देखते हैं। घोटुल में जवान लड़के-लड़कियों को एक दूसरे के साथ समय बिताने का और से एक दूसरे को समझने का मौक़ा मिलता है। घोटुल में आने के बाद लड़के बड़ी मेहनत से अपने हाथों से लकड़ी के कंघे बनाते हैं और फिर सभी लड़कियों को उनकी पसंद के कंघे भेंट करते हैं जबकि लड़कियाँ लड़कों को रंगीन पंख देती हैं। लड़के ख़ुद भी कंघे पहनते हैं पर उनके अपने कंघे लड़कियों को दिए जाने वाले कंघों की अपेक्षा बड़े होते हैं। एक बार किसी लड़की को जो कंघा मिल जाये, वह उसे स्वीकार कर लेती है – आपस में कंघों की बदली नहीं होती। घोटुल में आने वाले हर लड़के और लड़की को अपना जीवन-साथी चुनने की छूट होती है। इस सामाजिक स्वीकृति के कारण तमाम गोंड नवयौवनाएँ और नवयुवक यहीं से अपने वैवाहिक जीवन की भी शुरूआत करते हैं। कोई भी लड़की सभी लड़कों से मिले कंघे इस्तेमाल कर सकती है। हाँ, अगर किसी लड़की ने किसी लड़के से शादी कर ली, तो अपने पति के हाथों बना कंघा छोड़कर बाक़ी प्रेमियों के कंघे वापस कर देती है।
विकसित और आधुनिक कौन?
छत्तीसगढ़ के किसी गाँव में विशाल जब पहले-पहल पहुँचता, तो उसके जैसे पढ़े-लिखे, शर्ट-पैंट पहने व्यक्ति को देखकर आदिवासी बुज़ुर्ग अक्सर कहते – “भैया सब सुधर गए, लेकिन गोंड नहीं सुधरे!”
विशाल को समझ नहीं आता कि वे ऐसा क्यों कह रहे हैं। बात को सतही ढंग से न लेकर उसे गहरा कुरेदने की कोशिश की तो जाना कि बुज़ुर्ग लोग इस तरह की बातें अपने गाँव में आने वाले सरकारी अधिकारियों से सुना करते थे उन ग्रामीण आदिवासियों के बारे में जो—बक़ौल इन अधिकारियों के—सरकारी योजनाओं के हिसाब से फसल चक्र नहीं अपनाते हैं, ग्रामसभा में नहीं जाते हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई का ध्यान नहीं रखते हैं, सरकारी अस्पतालों में उपचार नहीं कराते हैं, अपने त्योहारों में दारू पीकर नाचते हैं, और महीनों तक आस-पास के गाँवों में मढ़ई-मेला मनाते हैं!
अब इसे त्रासदी ही कहेंगे कि बिलकुल ऐसी ही बातें ऋचा ने भी सीतापुर ज़िले में संगतिन किसान मज़दूर संगठन के साथियों से सुनी हैं – शहर से आये व्यक्ति गाँव के लोगों को इतनी बार बेवक़ूफ़ या गँवार कहकर चले जाते हैं कि वहाँ के लोग ख़ुद को भी अक्सर इन्हीं संज्ञाओं से सम्बोधित करने लगते हैं। इन सम्बोधनों के पीछे यही सोच रहती है कि अगर गाँव के लोग आँखें मींचकर सरकारी अधिकारियों और एन.जी.ओ. कार्यकर्ताओं की नसीहतें नहीं मानेंगे तो कभी न “सुधर” सकेंगे!
भला यह कैसा सुधार हुआ कि जिन शहरों में पहलू ख़ान पर गाय का माँस बेचने का झूठा आरोप थोपकर उन्हें जान से मार दिया जाता है, जहाँ से निकले नेता धर्म की आड़ में दंगे फैलाते हैं, जहाँ लड़कियों और महिलाओं पर होने वाले शारीरिक और लैंगिक अत्याचार सारी हदों को पार कर चुके हैं, जहाँ अलग जाति में किसी का प्रेम सम्बन्ध होने पर बेरहमी से ‘हॉनर किलिंग’ कर दी जाती है, जहाँ दलित एवं पिछड़े वर्गों के साथ हैवानियत से बर्ताव किया जाता है – ठीक उन्हीं शहरों से निकले लोग गाँव में रहने वाले दलित और आदिवासी साथियों की जीवन शैली पर अपनी बिन-माँगे टिपण्णी देते हैं और उन्हें बार-बार अपने से नीचा आँकते हैं। सुधार, आधुनिकता, विकास, और शिक्षा के नाम पर होने वाले इस घोर अज्ञान और अन्याय को हम एक समाज के बतौर हिंसा की संज्ञा देने की हिम्मत कब कर पाएंगे?
हर मौसम में यह शहर
चढ़ाये रहता है अपनी आँखों पर
एक काला चश्मा
जिससे यह भ्रम होता रहे
कि चश्मे के उस पार से
इसे दिखता है सबकुछ,दरअसल शहर के पास आँखें नहीं हैं
चेहरे पर एक लम्बी नाक भर है।
[. . . .]
यह इंसानों की गंध नहीं पहचानता
इसलिए सूँघता है दूर से ही
सड़क पर या गलियों में,
झुण्ड में या फिर अकेले
राह चलती लड़कियों की गंध
और टूट पड़ता है एक साथ
जैसे कुत्तों के झुण्ड को
दिख गया हो
कोई माँस का टुकड़ा।
यह पहचान लेता है
कन्या-भ्रूण की गंध
जैसे पहचानता है
धूल की गंध
लोहे की गंध
बारूद की गंध
माँस की गंध
ख़ून की गंध।
मगर मिट्टी की गंध
बारिश की गंध
पेड़ की गंध
जंगल की गंध
आदमी की गंध
सिर्फ़ इसकी कल्पना में है।4
In all the seasons, this city
puts a pair of dark sunglasses
on its eyes
to give the impression
that it can see everything
from the other side of those glasses.
In truth, this city has no eyes.
All it has is one long nose.
[. . . .]
This city does not recognize
the scent of humans
So it sniffs from a distance
on the street or in the lanes
the scent of young women passing by
in clusters or alone
and pounces upon them all at once
like a pack of dogs, that
has spotted
a piece of meat.
This city can recognize
The scent of female foetuses
Just like it can tell
The scent of dust
The scent of iron
The scent of gunpowder
The scent of flesh
The scent of blood.
But the smell of soil
the smell of rain
the smell of trees
the smell of forests
the smell of humans
exist only in its imagination.5
अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए हम ज़रा देर के लिए इस लम्बी नाक वाले ख़तरनाक शहर से दूर एक बार फिर घोटुल की ओर लौटते हैं —
O the kingdom of the unmarried!
You will never see that kingdom [anymore.]
Of housework you know nothing.
You went wandering in the fields,
Looking like a sarus crane.
Early morning you would go;
Evening you’d come home again.
O that beautiful ghotul!
Every day you went to clean it.
The road was like a jackal’s tail.
You used to go along that road.
In your left hand was a winnowing-fan,
In your right hand a broom,
At sunset you would go there.
You will never see that Raj again.
Now you are going to your husband’s house.
You have got no sense at all.
Your husband will curse you,
Your mother-in-law will curse you.
Holding your forehead you will weep.
You will remember the days of youth.
Then you will know what hardship is.
You have got no sense at all.6
हे अविवाहितों के राज्य!
इस राज्य को तुम अब कभी न देख सकोगे।
गृहस्थी के काम–काजों को तुम क्या जानो
तुम तो खेतों में डोलते
सारस की तरह
तड़के तुम निकल जाते
देर शाम वापस घर आते
वो खूबसूरत घोटुल!
तुम उसे रोज़ साफ़ करने जाते
उसी रास्ते से
जहाँ सड़क एक सियार की पूँछ थी
तुम्हारे बायें हाथ में एक सूप का पंखा होता
दाहिने में एक झाड़ू,
सूर्यास्त के समय वहाँ जाओगे
तो उस राज्य को अब न देख पाओगे
तुम अपने पति के घर जा रही हो
तुम्हें नहीं जानती अभी कि
तुम्हारा पति तुम्हें गाली देगा,
और सास देगी श्राप
तुम रोओगी अपना माथा पकड़े
याद करोगी अपनी जवानी के दिन
तब जानोगी कि कठिनाई किसे कहते हैं
अभी तुम्हें इसकी भनक भी नहीं है।
वेरियर एल्विन द्वारा गोंडी भाषा से अंग्रेजी में अनूदित इस गीत में उस मोटियारिन की वेदना है जो शादी होने के बाद घोटुल में बिताए बेफ़िक्र और सुहाने दिनों को बड़ी कसक के साथ याद करेगी। इस गीत में कुछ खोने का, कुछ छूटने का, एक अनोखा दर्द साँस ले रहा है! लेकिन आज की तारीख़ में अगर आप घोटुल के ऊपर गूगल सर्च करेंगे तो आपको इस दर्द का ज़रा भी आभास नहीं होगा। ज़्यादातर ऐसे मुख्य शीर्षक ही दिखेंगे:
“बस्तर की घोटुल प्रथा: स्त्री-पुरुष का यौन-मिलन स्थल…..”
“इस जनजाति ने अपने बच्चों को सेक्स की आज़ादी दी, लेकिन समाज भटक गया।”
“पहले मनाते हैं सुहाग रात, फिर करते हैं शादी…”7
इन सारे मुख्य शीर्षकों में घोटुल एक गहरी जीवन-शैली से उपजा दर्शन या पद्धति न होकर शहरियों की निगाह में सिर्फ़ शादी के पूर्व लैंगिक सम्बन्ध बनाने का वैध सामाजिक तरीक़ा बनकर रह जाता है। सेक्स – एक सपाट शब्द में छिपी ऐसी चाह जिसे “प्रगत” लोग प्रायः अपने तथाकथित विकसित समाज के रीति-रिवाजों के पिंजरों को तोड़कर पूरा तो करना चाहते हैं, लेकिन शायद ही कभी आज़ाद होकर वहाँ तक पहुँच पाते हैं। लेकिन यही सम्बन्ध ज़िन्दगी की एक बुनियादी अभिव्यक्ति के रूप में आदिवासी समुदाय सदियों से पूरी ज़िंदादिली और इज़्ज़त से जीते आ रहे हैं।
घोटुल का मुख्य उद्देश्य शिक्षा रहा है। इसे जीवन-कला भी कहा गया है – एक ऐसी कला जिसमें आजीविका के साधन, संगीत और नृत्य, घरेलू काम, शिकार करना, एवं लैंगिक और भावनात्मक नज़दीकियाँ सभी एक भरी-पूरी ज़िन्दगी का हिस्सा होती हैं। किन्तु जिन लैंगिक क्रियाकलापों को आदिवासी समुदाय नौजवानों को सिखाई जाने वाली ज़रुरी शिक्षा के रूप में देखते हैं, वही क्रियाएँ शहरी निगाह में मात्र सेक्स बनकर रह जाती हैं। ऐसी सोच को केवल पश्चिमी सभ्यता से निकली समझ कहकर टाल देना ग़लत होगा; दरअसल, यह सोच हमारे ब्राह्मणवादी और मनुवादी समाज में गहरे पैठी कुशिक्षा से जनित कमज़ोरी का भी बहुत बड़ा प्रतीक है।
कहते हैं, जब शहर के पढ़े-लिखे पुरुष बस्तर जैसे इलाक़ों में नौकरी के लिए आने लगे, तब वे भी आदिवासी नवयुवतियों से लैंगिक संबंधों की चाह में घोटुल में शामिल होने लगे। ख़ुद शादी-शुदा होने के बावजूद ऐसे तमाम पुरुषों ने मोटियारिनों से झूठ बोलकर विवाह रचाये और उन्हें उनसे संताने भी हुईं। लेकिन फिर तबादला होने के बाद यही लोग अपने आदिवासी परिवारों को छोड़कर चलते बने। बस्तर के बहुतेरे लोगों का मानना है कि ऐसे पुरुषों ने ही बाद में घोटुल की बदनामी भी की, और ऐसे ही तमाम प्रकरणों के बाद बार-बार यही सुनने में आने लगा कि “सब सुधर गए, लेकिन यह गोंड (आदिवासी) नहीं सुधरे”। जैसे-जैसे विकास के नाम पर “सुधारकों” का राज-काज बढ़ा, बस्तर के आदिवासियों के दिमाग़ों में भी यही बात बैठने लगी कि पढ़े-लिखे, अफ़सरनुमा लोग जो कह रहे हैं, वही सच है, तभी हम पिछड़े हैं। आदिवासी भी अपने को हीन दृष्टि से देखकर शहरियों की बातें दोहराने लगे। नतीजतन, आज की तारीख़ में कुछ अंदरूनी गाँवों को छोड़कर घोटुल लगभग ख़त्म ही हो गया है। इस प्रथा का—और ग्रामीण और आदिवासी समाज की ऐसी ही तमाम धरोहरों का—सुधार के नाम पर ख़त्म होना केवल ग्रामीण और आदिवासी समुदायों की ही क्षति नहीं हैं। इस तरह की संस्थाओं और मूल्यों का नष्ट होना हमारी कुल इंसानियत को पीछे धकेलकर हमारी समझ को, हमारी जीवन शैली को और ग़रीब बना देता है।
सवाल दर सवाल
घोटुल संस्था के बहाने जब हम विकास और शिक्षा की पूरी व्यवस्था पर विचार करते हुए इस लेख के लिए अपने लफ्ज़ तलाशने और तराशने लगे तो कितने ही सवाल हमारे मनों में कौंधने लगे। आज जब दुनिया में ब्लैक एक्टिविज़्म, दलित एक्टिविज़्म, तथा आदिवासी और मूलवासी समुदायों के संघर्षों—और उन संघर्षों से निकले विचारों—पर इतना कुछ कहा-सीखा-समझा जा रहा है, तब भारत और दक्षिण एशिया में आदिवासी जीवन, आदिवासी संघर्ष, और आदिवासी एक्टिविज़्म के बारे में शिक्षा का इतना गहरा अभाव क्यों?
आज संयुक्त राज्य अमरीका में हर स्तर का विद्यार्थी और शोधक ब्लैक लाइव्ज़ मैटर, ब्लैक एक्टिविज़्म, सिविल राइट्स मूवमेंट, और इंडिजेनस मूवमेंट्स के बारे में जानकारी रखता है। यही नहीं, पिछले तीस बरसों में तमाम अश्वेत विद्वानों ने मिलकर क्रिटिकल रेस थ्योरी को आगे बढ़ाया है। यह थ्योरी नस्लवाद को समझने में और उससे जुड़े तमाम ज्वलंत मुद्दों पर काम करने के लिए कारगर रही है और इसे आजीविका के संसाधनों, शिक्षा, स्वास्थ्य, और आवास जैसे बुनियादी हक़ों को लेकर होनेवाले भेदभाव पर शोध और ज़मीनी काम करने के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। इसी तरह भारत में डॉ. आंबेडकर दलित एक्टिविज्म के प्रेरणास्त्रोत रहे हैं, और नामदेव ढसाळ, राजा ढले, जे. वी. पवार जैसे विचारकों और कार्यकर्ताओं ने, तथा कांशीराम, मायावती, और रामदास आठवले जैसे राजनीतिक नेताओं ने उनके काम को आगे बढ़ाया है। लेकिन अचरज की बात है कि भारतीय स्कूली शिक्षा में आज भी आदिवासी विद्वानों, कार्यकर्ताओं, या आंदोलनकारियों के कोई नाम आसानी से नहीं मिलते। भारतीय पार्टियों की राजनीति देखें तो भी ऊपर से यही लगता है कि आदिवासियों द्वारा स्थापित मध्य भारत की गोंडवाना पार्टी को थोड़ा-बहुत छोड़कर आदिवासी नेतृत्व का एक बड़ा हिस्सा भा.ज.पा. या कांग्रेस जैसी पार्टियों से जुड़कर अपनी जुदा ताक़त खो रहा है।
भारत के अधिकांश शहरी और शिक्षित लोग या तो आदिवासी जीवन को हीन दृष्टि से देखते हैं, या फिर उसे एक रूमानी नज़र में क़ैद कर देते हैं। इन दोनों ही भावों में आदिवासी जीवन ग़ैर-आदिवासी जीवन के सन्दर्भ में एक अंतर बनकर रह जाता है। घोटुल भी ऐसा ही एक अंतर बन गया है। आज के दौर में जहाँ इन्सानी रिश्ते अपनी सहजता खो रहे हैं, जहाँ दो लोग एक दूसरे के साथ होकर भी अक्सर आपस में अपरिचितों की तरह रहने लगते हैं, जहाँ मनुष्य का लालच मौसम के बदलाव के रूप में सारी पृथ्वी का ख़ात्मा करने पर तुला है, जहाँ महिलाओं और अल्पसंख्यकों के ऊपर होनेवाले अत्याचार ख़ूंख़ार रफ़्तार से बढ़ रहे हैं! ऐसे कठिन दौर में हम उन आदिवासी समुदायों से कितना कुछ सीख सकते हैं जिन्होंने विकास के नाम पर होने वाले विनाश की सारी मार के बावजूद आज तक अपनी संस्कृति और पर्यावरण के बीच का संतुलन बनाये रखने की लड़ाई जारी रखी है। ऐसे जुझारू समुदायों की सांस्कृतिक धरोहर में समायी शिक्षा और ज्ञान को नैतिकपूर्ण ढंग से ग्रहण करके हमें अपने समाज के कितने ही ज़हरीले तत्वों से लड़ने की शक्ति मिल सकती है। सच्चाई तो यह है कि अगर तथाकथित शिक्षित समाज ने आदिवासी विद्वानों और वैज्ञानिकों की शिक्षा को ग्रहण करने में देर की तो हम काले चश्मे पहने शहरों की भाँति ख़ुद अपनी ही कुशिक्षा की हिंसा में भस्म हो सकते हैं।
जब कभी टकराती है
इसकी नाक से कोई आदिम गंध
एक आदमी निकल आता है
इसकी कल्पनाओं से बाहर
और यह शहर छूकर देखता है
उस आदमी की आँखें बड़ी हैं
मगर नाक है छोटी सी,
खुश होता है यह सोच
अच्छा है!
लम्बी नाक सिर्फ़ उसी के पास है
और गर्व से अपना सीना फुलाता है।
पूछता है छोटी नाक वालों को
होती होगी दिक़्क़त
गंधों को पहचानने में।
आदिम गंध से सना आदमी कहता है
जब हर चीज़ खड़ी हो एक साथ
अपने अनूठेपन पर बिना बोले
किसी की भिन्नता को
निम्नता के तराज़ू पर बिना तौले
तब क्या ज़रुरत है लम्बी नाक की?
क्या इतना काफ़ी नहीं
कि वह पहचानता है
पृथ्वी की आत्मा को,
पहाड़ की आवाज़ को,
समय की पीड़ा को,
ज़मीन की धमनियों में
दौड़ते रक्त के मर्म को
और पृथ्वी की देह से उठती इंसानी गंध को।8
Whenever a primeval scent
collides with this city’s nose
a man emerges from
its imagination.
This city touches his face
and discovers that the man’s eyes are big
but his nose is short.
Exhilarated, it thinks
That’s good!
Only it possesses a long nose.
Proudly puffing up its chest
it asks the short-nosed people
if they find it difficult
to recognize scents.
Says the man soaked in primeval scent
When everything stands together
without commenting on its own singularity
without placing difference
on the scale of inferiority
then what’s the point of a long nose?
Is it not enough
that he knows
The soul of the Earth
The voice of the mountains
The agony of Time
The heartache of the blood
running in the veins of the ground
And the scent of humans
rising from the body of this Earth.9
After Reading Jacinta . . .
A summary in translation
Vishal Jamkar, Richa Nagar
The above essay in Hindi emerged organically over the course of several months as we jointly engaged with Jacinta Kerketta’s submission to AGITATE!. It continued to find inspiration from her ideas and poetry as it grew from our verbal discussions into Vishal’s diary, and then into a co-authored reflection and essay. To try to convey in English all of the contents of what has evolved in the preceding pages seems far too mechanical to us. Therefore, we offer here a summary of our engagement with Jacinta, chiefly for those readers who do not read Hindi.
While working with a non-profit organization in India, Vishal was associated as a grassroots activist in the Bastar region of Chhattisgarh in India. This is the same region that Jacinta Kerketta writes about in her essay. In Bastar, Vishal’s NGO team was responsible for mobilizing more than 10,000 Adivasi (indigenous) and Dalit10 women from 110 villages through Self-Help Groups (SHG). SHG women formed an organization called the Mahila Shakti Sangathan in the Bhanupratappur Block. This Sangathan works with women and their families on the issues of gender, livelihood, and governance. Known in the popular media for its Left Wing Extremism, the Bastar region in Chhattisgarh is also unique for the rich culture of the Gond Adivasi community. Vishal’s reflections on his experiences of the politics of development and empowerment in Bastar resonated in strong ways with the lessons and insights that Richa has gained from her work since 2002 with members of what is now called the Sangtin Kisaan Mazdoor Sagnathan (SKMS), an organization of chiefly Dalit farmers and laborers in the Sitapur district of Uttar Pradesh.
Reading Kerketta’s writing about Bastar sparked a flood of memories for Vishal and led to a series of conversations between both of us about the violence of development, the production of the difference between the urban and the rural, the Adivasi and the non-Adivasi, and the imposed and internalized hierarchies of knowledge shaped by the dominant systems of education. In our essay, we work through these issues by focusing on one aspect of Adivasi lives in Chhattisgarh that Vishal came to grapple with quite centrally: the Ghotul.
Soon after Vishal arrived in Bastar, he came to realize that Ghotul as a social institution had a unique significance in the lives of the communities he was living with. He started reading about Ghotul through books available in English and Hindi, but there was so much that could only be learned through deep conversations with the Adivasi people of Bastar. At first, Vishal respectfully approached Kausalya Didi with his questions about Ghotul, but she shyly turned her face and avoided the question. Then he went to the men who also laughed it off. As their mutual relationships thickened, however, and as they sensed Vishal’s non-judgemental attitude towards Ghotul, both men and women began to open up about their memories and experiences of this institution.
The initial reluctance and resistance that Vishal encountered made him reflect hard on the mistrust that stands like a cement wall between the worlds of the Adivasi and non-Adivasi. He began to ask why some members of Adivasi communities often used the words of formally educated people from the cities to dismiss or ridicule their own rich ways of living – “Brother, over these years all communities have developed, but Gonds have not improved one bit!” This is exactly how many Dalit mazdoors and small farmers in the Sitapur district dismiss themselves – “When we ourselves are idiots, how can the government help us?”
In reality, when the so-called uneducated rural-based people from Adivasi and Dalit communities start sharing deeply about their ways of living and seeing the world, the complexity and sophistication of their arguments and theories can often challenge the work that emerges from the most premier academic institutions and think-tanks of the world. Furthermore, the professionally trained and educated cannot encounter this kind of knowledge in the absence of deep relationships of trust that refuse the violent hierarchies between the expert and the non-expert.11
A few words about Ghotul: Ghotul is a crucial social institution of the Gond, who are a prominent Adivasi community in India. Around the 5th and 6th Century A.D., Gonds began to spread from the southern to central and eastern parts of India. Lingo Pen, considered as the founder of the Gond tribe, organised his people in 750 clans and created Ghotul as a medium through which education and wisdom from the previous generations could be passed on to the young. Physically, Ghotul exists in the form of a mud and clay hut on the edge of the village. In this space, a facilitator accompanies a group of unmarried adolescent women and men. Cleanliness, discipline, and hard work are the premises of Ghotul. In the evening, young women and men start assembling around the Ghotul and dance. Young men offer beautifully carved combs that they make to propose a relationship, whereas young women offer colorful feathers to the men they desire closeness with. Many combs and feathers are proudly flaunted throughout the time when the young women and men share the space of Ghotul. Many times, this period marks the beginning of a long-term co-living by couples, which is socially sanctioned by elders.
A simple google search on Ghotul yields exotic headlines such as “Ghotul in Bastar: a meeting place for men and women for sexual pleasures” or “Ghotul: a place where pre-marital sex is sanctioned.” Ghotul—a rich ancient medium of co-learning holistically about such aspects of life as livelihoods, arts, music, dance, household work, hunting, emotional and sexual intimacies—is flatly reduced to a place where Adivasis have socially sanctioned pre-marital sex. The reductive assumptions and judgmental opinions of the so-called higher educated emanate not only from western thought; they are equally a product of brahmanical and manuvaadi frameworks that stifle Indian thought and practice. Indeed, according to the people of Bastar, it is the extremely negative representations of Ghotul by the non-Bastaris who started coming to Bastar for the government jobs in the post-independence period that led to the steady diminishing of this great institution. Today, Ghotul is only practiced in a few interior areas of Bastar. The retraction in the name of “development” of the practices and values embodied by Ghotul is a profound loss not only for the Gonds of Bastar. In fact, such disengagement from ancient wisdom and from celebration of the fullness of life impoverishes humanity as a whole.
Today, Dalit activism, Black activism, and movements of indigenous peoples have become major inspirations for intellectuals throughout the world. However, educational institutions throughout India and much of South Asia continue to be silent about Adivasi and indigenous knowledge and activism and the ways in which these communities have bravely struggled against the forces of destructive development for centuries. Due, in part, to these erased and unacknowledged contributions, the Gondwana Party of the Adivasis has lost its significance in central India. Many Adivasi political leaders have aligned with the two national parties, the Bharatiya Janata Party and the Congress, both of which are run by the people and ideologies of the dominant castes.
Today, the lives and worlds of Aadivasis are either romanticized or violently dismissed and erased. In none of these scenarios do we get an option to deeply learn and engage the wisdoms, theories, and epistemes that breathe in these communities. Today, when the so-called developed world or the mainstream is fissured by extreme hatred along such lines as caste, class, race, and religion; when the greed of human beings is devastating our planet in the form of climate change; when the relationships between people are increasingly becoming superficial, there is much to learn from the Adivasi communities who have never stopped fighting to maintain the precarious balance between conservation and utilization, and for the healthy sustenance of the human alongside all that is other than human. If the non-Adivasis fail to pay heed to our Adivasi teachers, scientists, and intellectuals even now, it may soon be too late to stop our worlds from burning in the fires of self-destruction.
—
Suggested citation:
Jamkar, V. and R. Nagar. 2020. “जसिन्ता को पढ़ने पर / After Reading Jacinta.” AGITATE! 2: http://agitatejournal.org/article/जसिन्ता-को-पढ़ने-पर/.
- छवियाँ www.outlook.com, www.quora.com, व www.sahapedia.com से साभार।
The three images used in this article have been taken from www.outlook.com, www.quora.com, and www.sahapedia.com respectively (in order of appearance). ↵ - जसिंता केरकेट्टा के कविता संग्रह, जड़ों की ज़मीन में प्रकाशित कविता “किसी ने नहीं देखा मुझे” से उद्धृत (पृष्ठ १२-१५) ↵
- Excerpt from Jacinta Kerketta’s poem, “No one ever saw me” (pp. 12-15), in Jacinta Kerketta, Land of the Roots, New Delhi: Bhartiya Gyanpeeth, 2018. Translated from Hindi by Richa Nagar. ↵
- जसिंता केरकेट्टा के कविता संग्रह, जड़ों की ज़मीन में प्रकाशित कविता “शहर की नाक” से उद्धृत (पृष्ठ ५६-६१) ↵
- Excerpt from Jacinta Kerketta’s poem, “The City’s Nose” (pp. 56-61), in Jacinta Kerketta, Land of the Roots, New Delhi: Bhartiya Gyanpeeth, 2018. Translated from Hindi by Richa Nagar. ↵
- Translated from Gondi language into English by Verrier Elwin (see Muria and their ghotul, pp. 614-615, Oxford University Press, 1947). Translated from English into Hindi by Richa Nagar. ↵
- सन्दर्भ : 24×7 Chhattisgarh. Chhattisgarh News, https://www.thelallantop.com, https://hindi.asianetnews.com. ↵
- जसिंता केरकेट्टा के कविता संग्रह, जड़ों की ज़मीन में प्रकाशित कविता “शहर की नाक” से उद्धृत (पृष्ठ ५६-६१) ↵
- Excerpt from Jacinta Kerketta’s poem, “The City’s Nose” (pp. 56-61), in Jacinta Kerketta, Land of the Roots, New Delhi: Bhartiya Gyanpeeth, 2018. Translated from Hindi by Richa Nagar. ↵
- Dalit, literally crushed, is a political identity and label embraced by the formerly “untouchable.” ↵
- For a detailed discussion of these points, see: Richa Nagar, in journeys with Sangtin Kisan Mazdoor Sangathan and Parakh Theatre, 2019, Hungry Translations: Relearning the World Through Radical Vulnerability, Chicago: University of Illinois Press. ↵
Article by: